राज कुमार सिंह का लेख : आगाज अच्छा, पर राह आसान नहीं
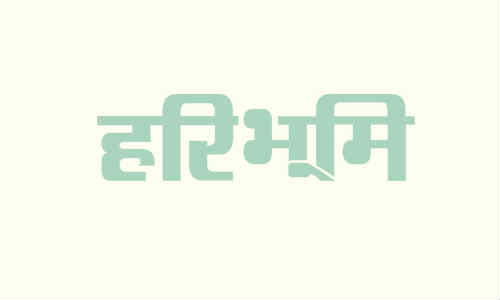
अगले लोकसभा चुनाव का अनौपचारिक बिगुल बज चुका है। 18 जुलाई को सत्तापक्ष और विपक्ष, दोनों ने ही क्रमश: दिल्ली और बेंगलुरू में शक्ति प्रदर्शन करते हुए चुनावी दंगल में ताल ठोक दी है। राष्ट्र चिंतन के बहाने शक्ति प्रदर्शन के लिए दोनों ही पक्षों ने पांच सितारा होटलों को चुना, जो दरअसल हमारे बदलते राजनीतिक चरित्र का ही परिचायक है। अगर घटक दलों की संख्या शक्ति का पैमाना है, तो बाजी सत्तारूढ़ भाजपा के हाथ मानी जा सकती है, जो अपने गठबंधन (एनडीए) का कुनबा, उसके रजत जयंती वर्ष में 38 तक पहुंचाने में सफल रही। वैसे पिछले महीने पटना में जुटे 17 दलों की संख्या को बेंगलुरू में 26 तक पहुंचाना (वह भी एनसीपी तथा बिहार में सत्तारूढ़ महा गठबंधन में सेंधमारी के साये में) विपक्ष की भी कम बड़ी उपलब्धि नहीं। आखिर वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद सत्ता के लिए बने यूपीए में मात्र 14 दल ही थे। वे भी धीरे-धीरे कम होते गए और 2014 में केंद्र की सत्ता से बेदखली के बाद तो यूपीए बिखर ही गया। राज्य-दर-राज्य राजनीतिक हितों और अहम के अंतर्विरोधों के बीच विपक्ष न सिर्फ अपना कुनबा बढ़ाने में, बल्कि गठबंधन का प्रभावशाली नामकरण करने में भी सफल रहा। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस, जिसका संक्षिप्त अंग्रेजी नाम ‘इंडिया’ बनता है, पर भाजपा की टिप्पणियां उसकी असहजता को ही दर्शाने वाली मानी जा रही हैं। कांग्रेसी से भाजपाई बने हिमंत बिस्वा सरमा इंडिया को अंग्रेजों द्वारा औपनिवेशक नामकरण बताते समय भूल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लागू कई योजनाओं के नाम में इंडिया शामिल है। वैसे इस नामकरण पर सवाल और विवाद की आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता।
भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे रहे यूपीए की जगह पीडीए की बजाय ‘इंडिया’ नामकरण में विपक्ष के जिन भी नेताओं की जो भी भूमिका रही हो, नारों और जुमलों के वर्तमान राजनीतिक दौर में वे बड़ा दांव चलने में सफल रहे हैं। वैसे इन दोनों गठबंधनों के मंच पर जुटे 64 राजनीतिक दलों का आंकड़ा हमारे यहां बहुदलीय लोकतंत्र के दलदल की ओर भी इशारा करता है। बेशक लोकतंत्र में राजनीतिक दल के गठन या उनकी संख्या पर कोई अंकुश नहीं है, पर यह अपेक्षा तो स्वाभाविक है कि उनका गठन किसी विशिष्ट विचारधारा के आधार पर किया जाए, जिसे अच्छे-खासे जनाधार का समर्थन भी हासिल हो। जनाधार संबंधी सीधी टिप्पणी दलों को अच्छी नहीं लगेगी, पर इस सच से कैसे मुंह चुराया जा सकता है कि दोनों ही गठबंधनों में शामिल 34 दल ऐसे हैं, जिनका संसद के किसी भी सदन में एक भी सांसद नहीं है। यह भी कि चार दल ऐसे हैं, जिनका प्रतिनिधित्व सिर्फ राज्यसभा तक सीमित है। एनडीए में ऐसे दलों की संख्या 24 है, जिनका लोकसभा में कोई सांसद नहीं। ‘इंडिया’ में ऐसे 10 दल शामिल हैं, जिनका किसी भी सदन में कोई सांसद नहीं। इसका यह अर्थ निकालना इन दलों के साथ न्यायसंगत नहीं होगा कि इनका कोई जनाधार नहीं है। सत्ता के बड़े खिलाड़ी नासमझ नहीं हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि जाति या समुदाय विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाले इन दलों के पास खुद जीतने लायक वोट प्रतिशत भले ही न हों, पर इनका 2-4 प्रतिशत वोट कड़े चुनावी संघर्ष में बाजी पलटने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। यही कारण है कि छोटे दलों के नेताओं की भी बड़ी मान-मनौव्वल की गई। जो दल अभी तक किसी गठबंधन में नहीं हैं, उन्हें येन केन प्रकारेण मनाने का उपक्रम चुनाव तक चलता रहेगा।
अब गठबंधनों की घटक दल संख्या से आगे की राजनीति-रणनीति की बात करते हैं। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने, तीन दशक लंबे अंतराल के बाद, जिस तरह अकेले दम पर बहुमत हासिल कर दिखाया था, उसके बाद विपक्ष में यह अहसास लगातार गहरा होता गया कि व्यापक विपक्षी एकता के बिना मोदी की भाजपा का मुकाबला मुमकिन नहीं। फिर भी एकता को सिरे चढ़ने में नौ साल लग गये तो इसलिए कि क्षत्रपों के बीच राजनीतिक हितों और महत्वाकांक्षाओं का तीव्र टकराव है, लेकिन बेंगलुरू में संयुक्त प्रेस कान्फ्रेंस के मंच पर लगा यूनाइटेड वी स्टैंड का बैनर उनकी सीमाओं की स्वीकारोक्ति ही था, वरना आम आदमी पार्टी बना कर कांग्रेस-भाजपा समेत परंपरागत राजनीति का ही विकल्प बनने चले अरविंद केजरीवाल उन्हीं नेताओं के इर्द-गिर्द नजर नहीं आते, जिन्हें वह कभी भ्रष्ट घोषित करते थे और कड़वा सच यह भी है कि ज्यादातर क्षेत्रीय दल परिवारवाद की जमीन पर ही खड़े हैं, पर यह विडंबना दोनों ही ओर नजर आती है। भ्रष्टाचार से दागी दामन का कटु सत्य भी यही है। परहेज किसी को नहीं है। सुविधानुसार तर्क गढ़ लिए जाते हैं। हां, मोदी की लोकप्रियता की लहर पर सवार भाजपा को चुनावी मुकाबले के लिए गठबंधन की गंभीर जरूरत पहली बार महसूस हुई है।
इसी कटु सत्य के आईने में देश की भावी राजनीति चलेगी और 2024 में केंद्र की अगली सत्ता का फैसला भी मतदाताओं को करना होगा। ऐसे में दोनों ही गठबंधन अपनी-अपनी सीमाओं के बावजूद संभावनाओं को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब जबकि इश्क और जंग की तरह राजनीति में भी सब कुछ जायज हमारे राजनेताओं ने मान लिया है तो चुनावी दंगल में हर संभव दांव नजर आएंगे। दूसरे कार्यकाल के उत्तरार्ध की फिसलन के बावजूद इसमें दो राय नहीं कि आज भी नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लोकप्रिया नेता हैं। फिर भी भाजपा ने चुनावी बिसात बिछाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने तो दलित वोटों को रिझाने में कसर नहीं छोड़ी गई। अब जबकि द्रोपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं तो आदिवासी वोटों पर भाजपा की नजर रहेगी ही, पर चुनावी तीर तो हर दल के तरकश में होते हैं। विपक्ष के नेतृत्व का फैसला तो अभी होना है, पर अपने गृह राज्य कर्नाटक में सर्वशक्तिमान भाजपा से सत्ता छीनने में कांग्रेस के दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब जबकि अल्पसंख्यक मतदाता क्षेत्रीय दलों का मोह छोड़कर कांग्रेस की ओर लौटने की सोच रहे हैं तो खड़गे के चलते दलित ऐसा क्यों नहीं सोचेंगे? हां, मुद्दों पर अवश्य घमासान मचेगा। भाजपा के तरकश में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के आजमाये हुए तीर तो हैं ही, विदेशों में भारत का गौरव बढ़ाने का गुणगान भी उनमें जुड़ गया है। दूसरी ओर अच्छे दिनों का अंतहीन इंतजार से लेकर बेरोजगारी और महंगाई की मार विपक्ष के प्रमुख मुद्दे होंगे। ऐसे में असल चुनावी कसौटी सुनियोजित-समन्वित रणनीति होगी, जिसे अंजाम देने में संगठनात्मक ढांचा और क्षमता निर्णायक साबित हो सकती है।
(लेखक- राज कुमार सिंह स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
